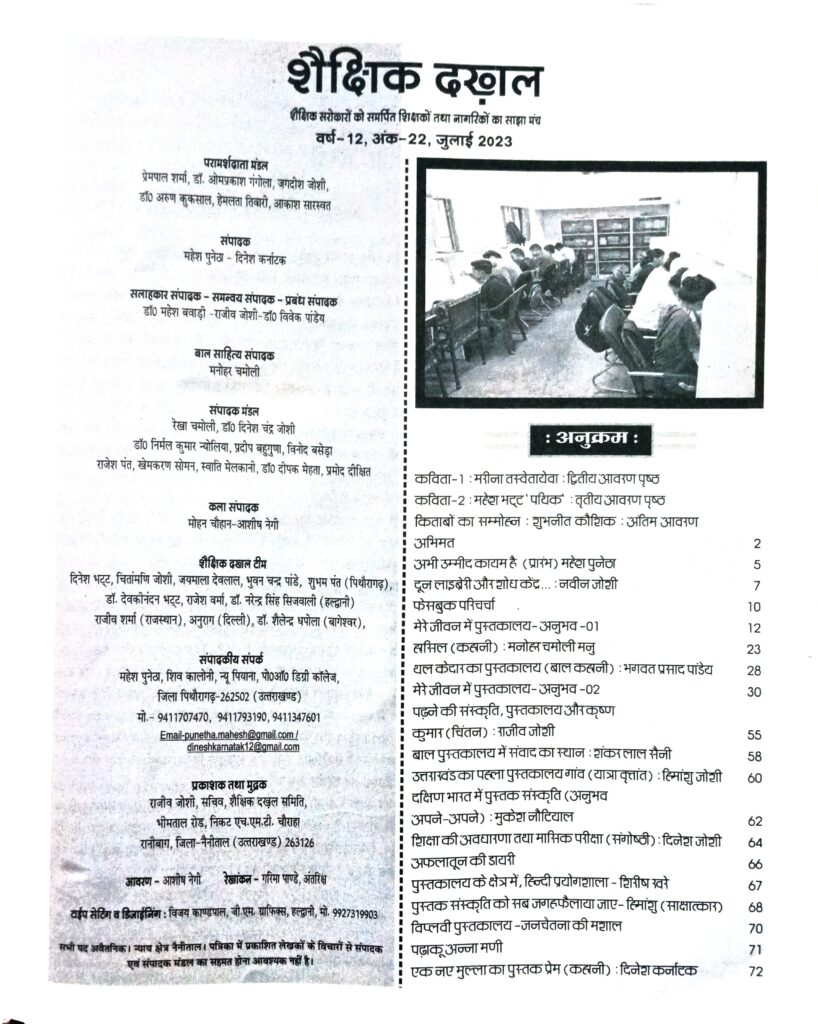शैक्षिक दख़ल का नया अंक : जुलाई 2023
शैक्षिक दख़ल शैक्षिक सरोकारों को समर्पित शिक्षकों तथा नागरिकों का साझा मंच है। विविध गतिविधियों में एक प्रकाशन भी दख़ल का काम है। फिलवक़्त पिछल बारह सालों से शैक्षिक दख़ल छमाही पत्रिका का प्रकाशन कर रही है। पत्रिका का नाम भी शैक्षिक दख़ल है। नवीनतम अंक 22वां प्रकाशित हो गया है। जुलाई 2023 के आलोक में यह अंक भी मेरे जीवन में पुस्तकालय-03 है। पिछले दो अंकों में बेतहाशा पाठकों, साहित्यकारों और विद्यार्थियों ने अपने संस्मरणात्मक आलेख भेजे। इस बार का अंक भी पुस्तकालय का जीवन में महत्व पर केन्द्रित है। कवर पेज शानदार है। मशहूर शिक्षक एवं कलाकार आशीष नेगी ने इसे तैयार किया है। पत्रिका में रेखांकन गरिमा पांडे और अंतरिक्ष के हैं ।
भीतर के आवरण में मरीना तस्वेतायेवा की कविता बच्चे है। बच्चे सूरज हैं। बच्चे सुकून हैं बच्चे पहेलियों का नाजुक संसार है। (पूरी कविता लेख के साथ छाया के तौर पर संलग्न हैं।)

इस अंक के अनुक्रम पर दृष्टि डालें तो प्रमुख रूप से मरीना तस्वेतायेवा की कविता बच्चे को पढ़ा जा सकता है।
अन्तिम भीतरी आवरण में नई किताब की गंध कविता महेश भट्ट ’पथिक’ की है। महेश किताब की गंध के वशीभूत उसकी तुलना कस्तूरी, चन्दन, गुलाब और रातरानी से करते हैं। यूँ कहा जाए तो उनके जैसे सभी पाठकों को किताब से आती गंध सबसे उम्दा लगती ही होगी।
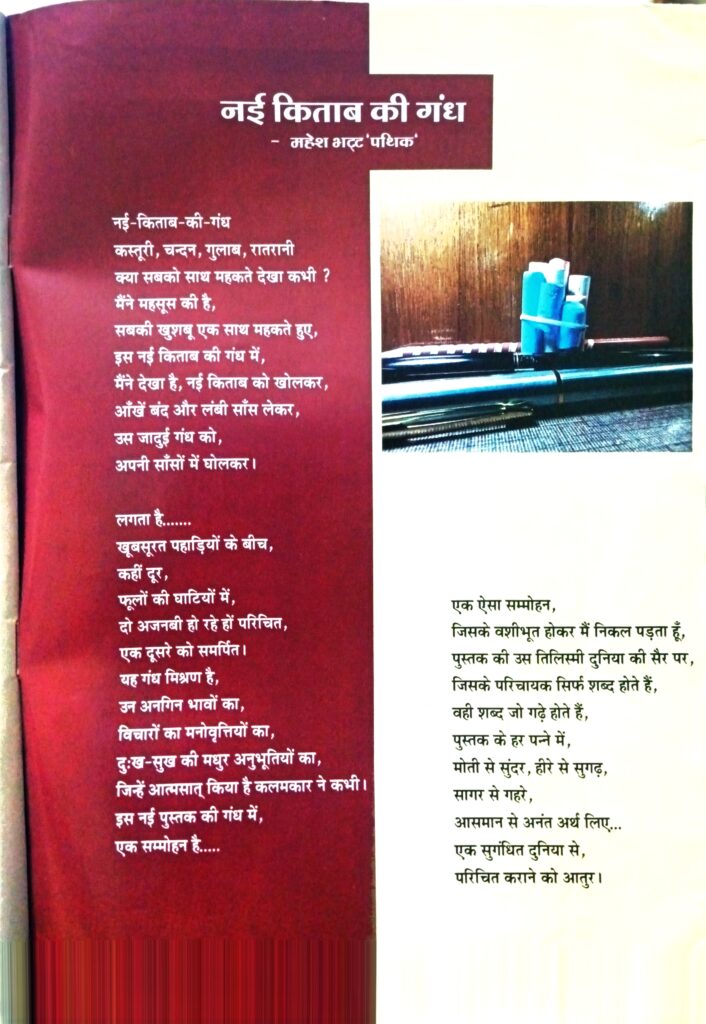
बाहरी अन्तिम आवरण पर किताबों का सम्मोहन शुभनीत कौशिक का संस्मरण है। उन्होंने संक्षेप में बताया है कि कैसे किताब उनके जीवन का कैसा और कितना हिस्सा है। अभिमत के जरिए भोपाल के राजेश उत्साही, जयपुर के दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, पिथौरागढ़ के दिनेश और उत्तरकाशी के सुंदर शिक्षार्थी की राय छपी है।
प्रारम्भ स्तम्भ के तहत संपादकीय में महेश पुनेठा लिखते हैं-
“पुस्तकालय अब संस्था के रूप में समाप्ति की ओर है। लखनऊ शहर में रहते हुए, जिन पुस्तकालयों से समृद्ध हुआ, वे आज दुर्दशा को प्राप्त हैं। इतने लंबे जीवन काल में पुस्तकों का जो निजी संग्रह बन गया है, अब उसको लेकर आशंका रहती है कि इनका होगा क्या, कैसे इन्हें भविष्य के लिए उपयोगी संस्था / व्यक्ति के सुपुर्द किया जाए। अब घर में पुस्तकों व पत्रिकाओं के लिए जगह बची नहीं है। पत्रिकाओं का बड़ा जखीरा सफाई-पुताई में नष्ट होता रहता है। सुपात्र तलाशने पर भी नहीं मिलते।“
पढ़ने की आदतों को लेकर हिंदी समाज में पहले से ही बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं रही है। हिंदी के वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव द्वारा अपने फेसबुक में व्यक्त की गई उक्त चिंता स्थिति की और अधिक भयावहता की ओर संकेत करती है। सच है कि आज स्कूल की समय सारिणी में पुस्तकालय के पीरियड के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि पीरियड हैं भी तो बच्चों को अपनी पसंद की किताबें पढ़ने का अवसर बहुत कम मिलता है। वहाँ बैठकर भी पाठ्यपुस्तकों या प्रतियोगिता साहित्य को पढ़ने पर बल दिया जाता है। अधिकांश स्कूल-कॉलेजों में किताबें आलमारियों या संदूकों में बंद देखी जाती हैं। खो जाने या फट जाने की डर से पुस्तकालय प्रभारी शिक्षक बच्चों को उनसे दूर ही रखते हैं। स्कूलों में पुस्तकालय सजावट की चीज से अधिक नहीं हैं। कभी-कभार बच्चों को उसे दिखाने भर के लिए वहाँ ले जाया जाता है। जैसे पुस्तकालय न होकर कोई संग्रहालय हो।
पुस्तकालयों के प्रति उदासीनता का आलम इससे अधिक क्या हो सकता है कि कुछ साल पहले पिथौरागढ़ के एक डिग्री कॉलेज में छात्रों को पुस्तकालय में अच्छी और नवीनतम किताबों की खरीद की जाने के लिए एक माह से अधिक समय तक आंदोलन करना पड़ा बावजूद इनकी इस माँग को पूरा नहीं किया गया। जिम्मेदार लोगों द्वारा “ पाठ्यपुस्तकों से इतर पुस्तकों की जरूरत ही क्या है, आखिर कौन पढ़ रहा है, उन किताबों को।“ जैसे हास्यास्पद बयान दिए गए।

प्रेरणा स्तम्भ के तहत नवीन जोशी ने दून लाइब्रेरी और शोध केंद्र की रोचक व प्रेरक कहानी का रोचक विस्तृत विवरण लिखा है। वह लिखते हैं-
दून लाइब्रेरी के बनने और यहाँ तक पहुँचने की कहानी रोचक ही नहीं, सपना देखने और उसके लिए समर्पित अभियान चलाए रखने की प्रेरक कहानी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति पद मुक्त होकर जब प्रो बी. के. जोशी 1998 में देहरादून जा बसे तो उनके भीतर वर्षों से बैठा बेहतर सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का सपना कुनमुनाने लगा। अमेरिका में अपने शोध – अध्ययन के दौरान वहाँ के विश्वविद्यालयों और विभिन्न शहरों के समृद्ध पुस्तकालयों को देखकर उनके मन में यह सपना बीज रूप में आ बैठा था। देहरादून में कोई अच्छा सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं था । इसलिए उन्हें जरूरत पड़ने पर मसूरी के राष्ट्रीय लालबहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के पुस्तकालय जाना पड़ता था। इस सपने की चर्चा 2005 में उन्होंने अपने लेखक मित्र एलन सेली और कवि-प्राध्यापक अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा से की। दोनों ने उन्हें उकसाते हुए पूछा- ’तो शुरू क्यों नहीं हो जाते ? ’ यह इतना आसान नहीं था। कोई भी अच्छा सार्वजनिक पुस्तकालय भारत में बिना सरकारी या सांस्थानिक सहायता के नहीं खोला जा सकता। शुरू भी कर दिया जाए तो चल नहीं सकता। तो, मित्रों के कहने पर जोशी जी ने पुस्तकालय खोलने के लिए एक प्रपत्र तैयार किया और तीनों मित्र उत्तराखंड सरकार के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव एम. रामचंद्रन से मिले। वहाँ से न केवल प्रोत्साहन मिला बल्कि एक विस्तृत योजना – पत्र बनाने को कहा गया। रामचंद्रन के समर्थन और सहयोग से योजना – पत्र आगे बढ़ा।’’
फेसबुक चर्चा -22 का कुछ हिस्सा इस अंक में है। विषय था- क्या पढ़ने के पीछे भी अब लाभ-हानि का दृष्टिकोण काम करने लगा है? इस परिचर्चा में प्रमुख रूप से राजेश उत्साही, रवि रौशन कुमार, ममता पंत, विकास नैनवाल, मुंतजिर अकरम, राजू मस्ताना, गिरीश चंद्र पांडेय, प्रमोद दीक्षित, रश्मि रावत, नरेन्द्र बंगारी और दिनेश कर्नाटक की राय शामिल हुई है।
इस अंक में मेरे जीवन में पुस्तकालय पर अनुभवजनित संस्मरण प्रचुर मात्रा में शामिल हुए हैं। एक-एक अनुभव जीवंत है। यथार्थ से भरा पूरा है। कौशल पंत किताबों वाला टिंडल कोना के तहत लिखते हैं-
यूँ तो बचपन से ही घर में पढ़ने का माहौल था। पिताजी का बिल गणित की बारीकियों को मजबूत करने में रहा और मेरी माँ हर कोशिश करती की मेरी लिखावट कैसे भी सुधर जाए। टाँकेदार लिखने की कला में पिताजी का पूरे गाँव में मान था और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी हर शाम रसोई में माँ के साथ बीतती। माँ को मेरा लेखन साफ ना होने का फिक्र सताता था, इसलिए टाँकेदार लिखना सिखाने के चलते रोटी में ना जाने कितने टाँके लगाए होंगे ये तो मेरी माँ ही जानती है। पास बैठाकर चकले पर फैली रोटी में अक्षरों को आकार देना, ये रोज का काम बन गया था। मैं इस जिद में कागज पर पेंसिल चलाता की मुझे रोटी में भी लिखना है। बार-बार रोटी में आकृति बनाना और फिर दुबारा से लेई बनाने में जितना वक्त जाया होता, उससे बेहतर उस रोटी को तवे में सेक दिया जाता था। इन बिना फूली रोटियों का भोग भी माँ ही किया करती थीं।
माँ ने ना जाने कितनी बार ’अ से अनार, आ से आम वाली रोटियाँ’ खाई होंगी, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं मगर मुझे रोटियों में कलाकारी दिखाने का मौका तीन से ज्यादा रोटियों में नहीं मिल पाता था। इससे मुझे बाद में माँ की डाइट का पता चला। खैर सुंदर लेखन का वह उच्च स्तर में आज भी नहीं छू पाया हूँ और आज भी स्थिति वही है, बस टाँके अब कलम से लिखे अक्षरों पर तिरछे लगते हैं।
संजय कापड़ी कृत ‘दीवार पत्रिका से बनी पुस्तकों की दुनिया की समझ’ भी पठनीय संस्मरण है। वे लिखते हैं-
आधुनिकता के इस दौर में जब मानव जीवन मोबाइल फोन की चाहरदीवारी तक सीमित रह गया है, पुस्तकें ही हैं जो हमें इस घुटन और अकेलेपन के कुएं में धकेले जाने से बचा ले जाएँगी। अपनी कहूँ तो जितना मैं इस जीवन को समझ पाया हूँ, उनमें मेरे व्यक्तिगत अनुभव तो शामिल रहे ही हैं, पुस्तकों का भी इसमें बराबर का योगदान रहा है। एक शिक्षक की तरह पुस्तकें और समाज दोनों ही हमें सिखाते हैं। कई बार समाज हमें कई प्रश्नचिन्हों के साथ आत्ममंथन की तरफ ले जाता है, उस समय पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती हैं और कुछ हद तक इन प्रश्नों पर विराम लगाती हैं।
ललित पांडेय कृत पहली बार असल में पुस्तकालय के दर्शन में वे लिखते हैं-
संवेदनाएँ, रोचकता और जिज्ञासा सबका उत्तर किताबों के पास है और किताबें हैं तो फिर सफलता बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। जितना ज्ञान में हमारे आरंभ के पुराने साथियों के पास देखता हूँ, मैं बस देखता रह जाता हूँ। यह बात बयाँ नहीं हो सकती और मैं कभी नहीं सकता। महीने के आखिर में एक बुक मीट होती है, जिसमें पढ़ी गई किताबों पर चर्चा की जाती है यह माहैल अलग है। सीमांत जैसे क्षेत्र में तो कल्पना से परे। यहा कारवाँ बस चल रहा है और आगे भी लगातार यूँ ही चलता रहेगा।
संचिता जोशी कृत कई बच्चों को तो नींद भी आ जाती में वह लिखती हैं-
मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। टाइम टेबल में एक हफ्ते में पुस्तकालय के दो पीरियड होते हैं। लाइब्रेरी मैम हमें बुलाने आती हैं। पुस्तकालय में हमें एक-एक किताब मिलती है, जो प्रायः पजल की होती है। हम बीच में लगी हुई बड़ी मेज के चारों ओर बैठकर पजल सॉल्व करने लग जाते हैं। कभी-कभी कहानियों की किताबें भी मिल जाती हैं, जो छोटे बच्चों की होती हैं। हमें उसकी समरी लिखनी होती है। किताबें छोटे बच्चों की अधिक होती हैं।
एक दिन मैडम ने हमें एक कहानी बनाने को कहा। मैंने कहानी बनाई। मैडम को दिखाई तो उन्हें पसन्द नहीं आई। उन्होंने कहा कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, यह नहीं लिखा है। यह कहानी मेरी लाइब्रेरी की कॉपी में चिपकी है। पसंद आने पर किताब घर को भी मिल जाती है। मुझे पसन्द नहीं आती। मैं आज तक कभी घर नहीं लाई ।
कक्षा-5 से पहले हम लाइब्रेरी कभी नहीं गए। किताबें हमारी कक्षा के ही एक कोने पर एक रैक में रखी रखती हैं। हमें वे किताबें एक बार मिलीं थीं। पुस्तकालय के पीरियड में हमें या तो कुछ पढ़ा दिया जाता था। कभी-कभी आँख बंद करके सो जाने को कहा जाता। कई बच्चों को तो नींद भी आ जाती थी। कक्षा 6 से ही हमें पुस्तकालय देखने को मिला। लेकिन मुझे आज तक कोई किताब याद नहीं आती। उससे अधिक किताबें मुझे एपीएफ की लाइब्रेरी से मिली। वहाँ किताबें खुली रैक में रखी थी। वहाँ विनोद अंकल मिले। उन्होंने हमसे कई सवाल किए। जैसे-कैसी किताब चाहिए, क्या पढ़ा है? आदि। फिर हमें बहुत किताबें मिलीं। हमने कुछ वहीं पर बैठकर पढ़ी। कुछ घर भी लाए। हमारे घर पर भी किताबें हैं। मैंने तोत्तोचान, कुछ यूँ रचती हैं हमें किताब, अंधेरे के पार, रस्टी के कारनामे, रूस्तम और सोहराब, स्वामी और उसके दोस्त, प्रेमचंद की कहानियाँ, मोइन और राक्षस, गिजूभाई की कहानियाँ पढ़ी हैं।
तब से कभी पुस्तकालय नहीं गए में अपने अनुभव लक्षिता जोशी कुछ इस तरह से बताती हैं-
मैं कक्षा-5 में पढ़ती हूँ । पुस्तकालय के पीरियड में सर हमें अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं। हमारे कक्षा के कोने पर एक लकड़ी की रैक में किताबें होती हैं। वे हमें कभी नहीं मिलीं। वैसे तो प्राइमरी वालों को लाइब्रेरी नहीं ले जाते लेकिन एक बार जब मैं कक्षा 4 में पढ़ती थी पता नहीं कैसे हमारा भी नंबर आ गया। सर हमें वहाँ ले गए। वो बहुत बड़ा कमरा था। लाइब्रेरी मैडम ने हमें एक-एक किताब दी । हमने जल्दी ही खत्म कर दी। मुझे एक मजेदार कहानी मिली। जिसमें हिम्पोपोटोमस बहुत खाना खाता था । हमने किताब पढ़ने के बाद उसे आपस में बदलना शुरू कर दिया। पसंद नहीं तो फिर बदल दिया। कमरे में हल्ला हो गया। सर ने कहा कि जिसने, जो किताब पढ़ी है उसके बारे में बताओ। मेरे हाथ में जो किताब थी वह बड़ी अजीब थी। मैंने सोचा, मैं वही कहानी बता दूँगी। लेकिन मेरे से पहले वह कहानी किसी और ने बता दी। मुझे डर लग रही थी कि अब क्या बोलूँगी। तब तक घंटी बज गई। हम कक्षा में आ गए। तब से कभी पुस्तकालय नहीं गए।
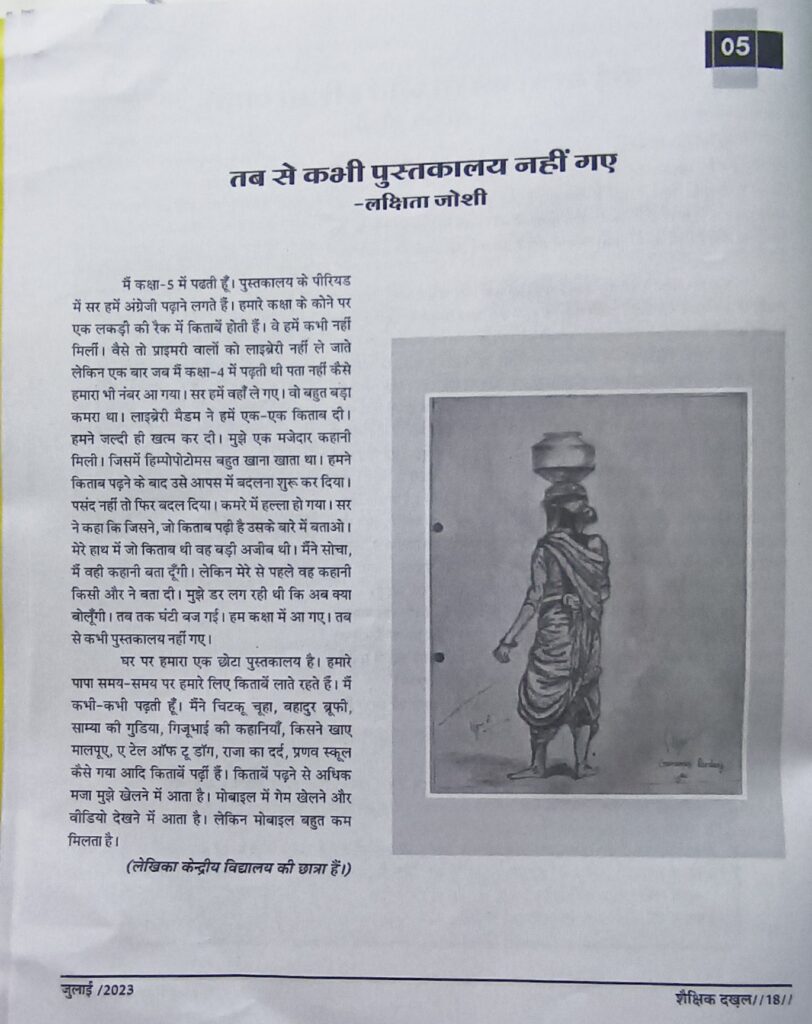
पढ़ाई वाला कमरा में निवेदिता सिजवाली लिखती हैं-
मेरे लिए पुस्तकालय मेरा दूसरा घर है। मैं बचपन से ही पुस्तक प्रेमी रही हूँ और इसका श्रेय मेरे पापा को जाता है। वह अक्सर ही हमारे लिए किताबें लाते रहे हैं। हमारे घर में एक पढ़ाई वाला कमरा है, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और बातचीत करते हैं। इस कमरे में एक व्हाईट बोर्ड है, एक अलमारी है और एक छोटी रैक है। हमारी जितनी भी किताबें हैं चाहे वह पाठ्यक्रम की हों या पत्रिकाएँ हों या कोई अन्य किताब हो सभी किताबें इसी कमरे की निवासी हैं (खैर जिस तरह से किताबों की संख्या बढ़ रही है, ये जगह उनके लिए कुछ कम पड़ती लग रही है)। ये कमरा एक चुंबक है और मैं इससे चिपकी हुई एक लोहे की कील। घर के इस छोटे से पुस्तकालय में पढ़ते हुए धीरे-धीरे मैं रचनात्मक कार्य कर पाना भी सीख रही हूँ, जैसे-कहानियाँ, कविताएँ, लेख, इत्यादि। इसके अलावा एक बार हस्तलिखित अखबार निकालने का प्रयास भी किया था। दोस्तों को या किसी को जन्मदिन पर किताब या पत्रिका भेंट करती हूँ। पर कहीं-कहीं पर जब पुस्तकों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर निराशा होती है। कई बार अपने कुछ सहपाठियों के रवैये को देखकर भी बुरा लगता है। परंतु अभी भी कुछ दोस्त ऐसे हैं, जिनके साथ पढ़ाई पर, पुस्तकों पर और एक बेहतर इंसान बनने पर बातचीत होती है और ये दोस्त कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए भी हमेशा प्रेरित करते हैं।
मानसिक विकास में एक अहम भूमिका के तहत दिशा पंत लिखती हैं-
हमारे स्कूल में भी एक पुस्तकालय है, किंतु वह केवल नाम का ही पुस्तकालय है। वहाँ से केवल पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं, पुस्तक पढ़ने का कोई विकल्प नहीं हैं। हाँ, जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है तब 6-7 बच्चों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज विद्यालय पुस्तकालय को महत्व नहीं देते हैं, जबकि पुस्तकालय या कहें पुस्तकें बच्चों की मानसिक विकास में एक अहम भूमिका निभाती हैं। नई-नई पुस्तकें पढ़ने से बच्चों के विचारों में परिवर्तन आता है।मैंने भी जब तक अपनी पाठयक्रम की पुस्तकें ही पढ़ी थी तब तक मैं केवल एक सीमित दायरे तक ही सोच पाती थी। मुझे अन्य तथ्यों का ज्ञान नहीं था किंतु जब मैंने उसी विषय पर अपने बड़ों द्वारा दी गई अलग-अलग पुस्तकें पढ़ी तब मैं तथ्यों का सही आकलन कर पाई। अपने स्वयं के विचारों को जन्म दे पाई। पिछले साल मैंने एकलव्य प्रकाशन से प्रकाशित ’अदृश्य लोग’ नाम की एक किताब पढ़ी तब मेरी सोच में भारी परिवर्तन आया। मैंने बहुत अधिक किताबें पढ़ी हैं, ऐसा तो नहीं कहूंगी किंतु मुझे लगता है कि जब एक किताब का ही किसी व्यक्ति की मानसिकता पर इतना गहरा प्रभाव पड़ सकता है तो व्यक्ति यदि अलग-अलग किताबें पढ़ें तो वह उससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता। केवल अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ने से व्यक्ति को केवल साक्षरता मिल सकती है, किंतु वास्तविक अर्थो में शिक्षित होने के लिए उसे अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए।
पहले सुन रखा था, अब जान लिया है…इस अनुभव को लिखा है आस्था ने। आस्था लिखती हैं-
मेरा पुस्तकालय के साथ सबसे पहले जुड़ाव मेरे अपने घर पर ही हुआ। मेरे घर में देशभर से पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। उनमें से मुझे बच्चों की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। उनमें बहुत सुंदर चित्र होते हैं, इन पुस्तकों के बढ़िया कहानियाँ होती थी, कविताएँ होती हैं और पहेलियाँ, पजल तथा कई प्रकार की मनोरंजक जानकारी होती है। परंतु जब मैं छोटी थी तो मैं कविताएँ या कहानियाँ नहीं पढ़ती थी, मुझे उनमें छपे चित्र बहुत अच्छे लगते थे। मैं उन्हें ही देखती रहती थी। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी रूचि कविता और कहानियों की तरफ भी बढ़ने लगी। फिर मैं उन्हें भी पढ़ने लगी। बहुत मजा आता है इन्हें पढ़कर। इस तरह से मेरी उनसे मुलाकात बार-बार होती है। है। मेरे पापा पवन चौहान एक लेखक हैं इसलिए हमारे घर में आए दिन किताबें व पत्रिकाएँ आती रहती हैं। मेरा उनके साथ जुड़ाव हमेशा ही बना रहता है। मुझे पुस्तकें पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूर ही नहीं हुई।
स्वर्ग एक पुस्तकालय ही होगा के तहत काव्या नौटियाल लिखती हैं-
मेरी नजर में पुस्तकालय वह स्थान है, जहाँ न केवल विविध प्रकार की पुस्तकों का संग्रह हो, बल्कि वहाँ पुस्तकों को सम्मान के साथ रखा भी जाए। याद आता है कि मेरे घर में पुस्तकों का जो संग्रह था, उसको मेरे पिताजी अपना पुस्तकालय कहा करते थे। भले वहाँ कुछ आलमारियाँ और एक कुर्सी-मेज का जोड़ा भर था। बचपन से मैंने देखा है कि जब भी मेरे माता-पिता को समय मिलता वह कोई ना कोई पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ जाते थे। इस प्रकार मेरा भी पढ़ने की परंपरा से परिचय बहुत छोटी उम्र में हो गया था। मेरी दादी मुझे गढ़वाल की कई लोक -कथाएँ सुनाया करती थी और मेरे नाना जी कृष्ण की बाल लीलाओं को कहानी के माध्यम से बताया करते थे। इस तरह मेरी कहानियों में रुचि जागृत हुई।
जब मैं कक्षा एक में थी तब मेरे पिताजी ने पहली बार मुझे अपने पुस्तकालय से एक किताब निकाल कर दी। वो किताब थी उन्हीं की लिखी हुई ’सफेद ऊन का गोला’। पहली बार मुझे ऐसी शानदार और जीवंत चित्रों से भरी एक आकर्षक किताब मिली थी, जो मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं थीं और जिसको मुझे होमवर्क की तरह नहीं पढ़ना था । पढ़ने का यह पहला और नया स्वाद कारगर साबित हुआ और उसके बाद मैं निरंतर बाल पत्रिकाएँ पढ़ने लगी। थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे पिताजी ने कई और किताबों से मेरा परिचय करवाया परंतु प्रमुखतः मैं लघुकथाएँ ही पढ़ती थी।
साहित्यकार भगवत प्रसाद पाण्डेय की बाल कहानी थलकेदार का पुस्तकालय भी इस अंक में हैं। कुछ अंश उनकी इस कहानी से यहाँ दिए जा रहे हैं-
सोर घाटी जितनी बड़ी थी, उतनी ही खूबसूरत। उसके एक तरफ सोडलेख और ध्वज के जंगल थे, तो ठीक सामने थलकेदार का विशाल और घना वन था । वहाँ के राजा शेरसिंह के स्वर्गवास के बाद उनके बेटे मृगेंद्र को थलकेदार वन की राजगद्दी मिली। नए राजा ने अपने राज्य को विकसित करने के प्रत्येक क्षेत्र में काम शुरू किए, जिससे थलकेदार जंगल के भी अच्छे दिन आ गए।
महाराज का यह भी मानना था, कि विकास के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। ‘सभी प्राणी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें’ यह सोच कर उन्होंने पहले अपने राज्य में पशु-पक्षियों की शिक्षा के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला एक स्कूल खोल दिया। उसी विद्यालय में महाराज की बेटी लाएंडरी भी पढ़ती, जो इस बार दसवीं में थी ।
प्रजा को बेहतर शिक्षा कैसे मिले ? इस बारे में राजा मृगेंद्र हमेशा सोचते रहते और पुत्री लाएंडरी को भी पढ़ाई का महत्व बताते थे । इतवार की बात थी। पाँच गुफाओं वाले पंच महल के आँगन में महाराज बैठे थे। सुबह की धूप का आनंद लेते-लेते, वे अखबार भी पढ़ चुके थे। तभी उन्होंने आसमान की ओर इशारा करते हुए अपनी पुत्री से एक सवाल किया- “बेटी, चंद्रयान-3 अभियान क्या है ?“
इस अंक में किशोरों और माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के संस्मरण भी है।
नेहा सैनी कृत अनुभव पढ़ने की मौज में वह लिखती हैं-
मेरे लिए स्कूल में पुस्तकालय का मतलब विद्यालय से बच्चों को प्रत्येक नए सत्र में पाठयक्रम की पुस्तकें प्रदान करने तक सीमित था। बाजपुर टाउन व अपनी प्राथमिक शाला में पुस्तकालय शब्द जैसा कुछ देखने को तो नहीं मिला लेकिन एक अनुभव जो पुस्तक से जुड़ता है अभी भी याद है- हम खेल खेल में ही पुराने रद्दी कागजों से किताब बनाते थे, जो बाद में पुस्तकों के साथ समय बिताने की अभिलाषा में तब्दील हुआ।
इसी तरह कक्षा ग्यारह की छात्रा आँचल अपने लेख में किताबों का ढेर नहीं होता पुस्तकालय में यह लिखती हैं-
शुरुवाती कक्षाओं में पुस्तकालय की बात तो छोड़ो समय पर अखबार या जो को भी पत्रिका मिलती उसमें किसी कहानी व पाठ्यपुस्तक व पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें मिलना भी मुश्किल रहा आत्मकथा को पढ़ना नहल छोड़ती। पाँच वर्ष पहले पुस्तकालय तो नहीं था। देर से ही सही मिलती भी तो पुरानी व आधी-अधूरी । विद्यालय की लेकिन बहुत सारा बाल साहित्य व चुनिंदा कहानियों के लिए हॉस्टल में समस्त अकादमिक गतिविधियों का केंद्र पाठ्यपुस्तक होने से शुरू हुए एकमात्र बुक कार्नर से मेरे बचपन का कहानी सुनने का शौक पाठ्यसहगामी पुस्तकों व पठनीय सामग्री का कोई अनुभव भी नहीं रहा। पढ़ने में तब्दील होने लगा।
ज्योति भट्ट अपने अनुभव यह लाइब्रेरी बच्चों के लिए नहीं है में कुछ इस तरह लिखती हैं-
मेरा पुस्तकालय शब्द से परिचय कक्षा पाँच में सरस्वती शिशु मंदिर बाड़ेछीना में हुआ, जहाँ एक लोहे की अलमारीनुमा रैक में तीन-चार किताबें रखी थी। प्रधानाचार्य कार्यालय में रखी इस रैक को मैं कौतूहल से देख रही थी, तभी मेरे प्रधानाचार्य ने कहा कि अब तुम दूसरे स्कूल में चले जाओगे तो इस पुस्तकालय के लिए कोई पुस्तक दे कर जाना। उस पुस्तकालय में मात्र तीन किताबें थी। मैं सोच में पड़ गई कि पुस्तकालय को पुस्तक देनी भी होती है? उसके पास अपनी पुस्तकें नहीं होती ?
खैर ! अब आचार्य जी की कही बात मेरे मन में घूमती रही और मेरे पास घर एक किताब “गुरु चेला“ थी जिसमें कुछ किस्से लिखे थे। वह मैंने पुस्तकालय को में दे दी। उसके बाद स्कूल बदल गया। शहर बदल गया। मैं अल्मोड़ा जी.जी.आई. सी. में पढ़ने लगी। यहाँ भी पुस्तकालय जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, एक कमरे में लोहे की अलमारियों में किताबें भरी थी, वही पुस्तकालय था। हालांकि उस पुस्तकालय से हमको कभी कोई किताब निकलते नहीं देखी। कक्षा ग्यारह में किसी कार्यक्रम के लिए विद्यालय की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा जाना हुआ और वापसी में शिक्षिका ने बताया कि जो यह राजकीय इंटर कॉलेज के बगल में ब्रिटिशकालीन इमारत है यह लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का नाम सुनते खुश हो गई। गेट से अंदर जाकर देखा बाहर बरामदे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे और अंदर कई अलमारियों में अलग-अलग तरह की किताबें रखी हुई थी। बीच में चार बड़े-बड़े मेज रखे थे, जिनके चारों तरफ कुर्सियाँ रखी थी। पहली बार जीवन में पुस्तकालय देखा और देखते ही रह गई। इतने में वहाँ के कर्मचारी आए और बोले कि यह लाइब्रेरी बच्चों के लिए नहीं है, पहले स्कूल की किताबें पढ़ो और उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। मैं भी लौट आई। सोचा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से फुर्सत मिले तो ही लाइब्रेरी का रुख किया जाए। बात आई गई हो गई।
एकता स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। वह अपने अनुभव मुझे दया आई इन किताबों पर…में लिखती हैं-
पुस्तकों से जुड़ाव का सफर हर किसी के पास होता है। हर कोई किताबों की यात्राओं को अपने-अपने स्तर में कर रहा होता है, कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाओ से मैं भी किताबों और पुस्तकालय से मिली। जब मैं कक्षा-9 में आई रा.इ.का देवलथल, जहाँ सामाजिक विज्ञान के अध्यापक महेश पुनेठा सर विषय की पुस्तकें पढ़ने के साथ-साथ हमें पुस्तकालय से अन्य किताबें पढ़ने को प्रेरित करते रहते थे। उन दिनों को अगर मैं याद करूँ तो मुझे खुशी भी होती है और दुःख भी क्योंकि मैं बहुत देर में पुस्तकालय से अपने को जोड़ पाई। यह मेरे लिए बहुत कठिन था विषय से बाहर की किताबों को पढ़ना। मैं डरती थी सवालों से, बोलने से और किताबों के नजदीक जाने से। मैं हमेशा से ही खुद को ढक दिया करती थी, उन चीजों से जो पुस्तकालय की दुनिया का रास्ता थी, लेकिन मैं बच भी नहीं सकती थी जाने से क्योंकि समाजिक विज्ञान की कक्षा सर हमें पुस्तकालय में ही पढ़ाते थे। सर का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह किताबों से होकर रचनात्मकता को हमारी कलम में उतारते थे, जो मेरे लिए ज्यादा चुनौती भरा था। जहाँ आज तक किताबों का लिखा रटकर लिखना मेरे लिए पीड़ादायक था अब खुद के विचारों को खाली पन्नों में मौलिकता से भरना था। उस बड़ी लंबी अनेक रचनाओं से दीवार पर टंगी पत्रिका, जिसे दीवार पत्रिका बोला जाता है, उसको अलग-अलग हाथों की कलम से रंगना था अब हमारी कक्षा के बच्चों ने। हर कोई लग गया अपने काम में कोई कविताओं के साथ खेल रहा है तो कोई लेखों में डूबा है व कोई चुटकुलों को खोज रहा है अपनी हँसी में । परंतु यह मेरे लिए बस एक होमवर्क था, जिसे मुझे कैसे भी निपटाना था।
नवमी अपने अनुभव काश ! बच्चों को मुफ्त में किताबें पढ़ने को मिलें में लिखती हैं-
बचपन की बेफिक्री से उठकर किताबों को टटोलने का मजा तब जाना, जब हमारे विज्ञान अध्यापक सुंदर सर ने एक किताब मेरे हाथों में थमाई। किताब का नाम था-विज्ञान औश्र हम। और लेखक देवेंद्र मेवाड़ी जी, जो विज्ञान के भयानक लगने वाले शब्दों को सरल बनाकर हम बच्चों को विज्ञान के तथ्यों से रूबरू कराते हैं। उस पहली किताब ने मुझे किताबों का मतलब बताया।
‘ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाईब्रेरी नहीं है, समझे मिस्टर ?’ अनुभवजनित संस्मरण डॉ० प्रकाश चंद भट्ट ने लिखा है। वे लिखते हैं-
क्या व्यवस्था पब्लिक लाईब्रेरी के लिए किताब चुनते समय किसान-धर्म से किताब चुन सकेगी। घास और गाजर घास की तरह, किताब और पेजों के संकलन में फर्क कर सकेगी। सपने देखने वाले सपनों के साथ मरते हुए पाए जाते हैं। गांधी भी सपनों के साथ मरे थे, भगत सिंह भी। वह भगतसिंह जिन की जेबों में किताबें ठुसी रहती थी। अंबेडकर, लोहिया, नेहरु आदि पुस्तकालय से बनते हैं।
कुछ दृश्यों पर थोड़ी नज़र डाली जाए तो फिर बात आगे बढ़े। इधर कुछ सालों से हॉस्पिटल में देवालय बढ़ने लगे हैं और नेशनल हाइवे पर मिलने वाली किताबों की दुकानें गायब हुई हैं। जहाँ किताबों की दुकानें होती थीं वहाँ आजकल मोबाइल एसिसीरिज़ की दुकाने हो गयी हैं। छोटे बड़े तमाम प्रकाशक व्यक्तिगत पुस्तक क्रय में दस फीसदी से चालीस फीसदी तक की छूट देते हैं पर वही छूट पुस्तकालय खरीद पर न जाने क्यों दस फीसदी रह जाती है। जिला पुस्तकालय, उपजिला पुस्तकालय बड़े-बड़े बागीचों की तरह मौसम के हिसाब से खुलते हैं। प्रोफेसर्स की टैक्सट बुक पर लाईब्रेरी का एक्सेसन नंबर क्यों दिखता है? बड़े-बड़े प्रोफेसरान कॉलेज लाईब्रेरी से सालाना कितनी किताबें इशू कराते हैं? पुस्तकालयों के रैक्स की पहली रो को छोड़ कर बाकी रो में लगे जाले क्या कहते हैं? ताजा भोजन करने वाले पुराने एडिशन की बासी किताबों को बड़ी संख्या में क्यों खरीद डालते हैं? दृश्यों की शृंखला को यहीं विराम देते हैं।
दीपक तिवारी अपने अनुभवों को कलमबद्ध करते हुए डॉक्टर तक पहुँच गया में लिखते हैं-
शिक्षा और किताब शब्द से सबका अलग-अलग रिश्ता है। किसी को बचपन से ही इसका सामीप्य प्राप्त होता है तो कोई बहुत सघर्षो के बाद इस तक पहुँच पाता है। मेरी जीवन यात्रा में इस बात का उत्तर भाग ही अधिक सटीक है। मेरे माता-पिता बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से रहे। वे पहली पीढ़ी के लोग थे, जो शहर की ओर पलायन कर गए थे, ताकि अपने और अपने ऊपर निर्भर अन्य लोगों को एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकें। जहाँ पिता गाँव के विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण थे, वहीं माता जी ने 8वीं कक्षा को बड़ी मुश्किल से नकल कर पास किया और इसके उपरांत अच्छी गृहणी बनकर शिक्षा प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देने लगी थी। वर्ष 1991 में मेरे पिता का प्रवास दिल्ली हुआ और वर्ष 1992 में मेरे जन्म के एक वर्ष पश्चात वर्ष 1993 में वह मुझे और मेरी माताजी को लेकर दिल्ली आ गए। गाँव से वह ना केवल हमें, वरन वहाँ की शिक्षा, रीति-रिवाज, जाति-व्यवस्था, रूढ़िवादी सोच सभी कुछ साथ लाए थे। समय के साथ मेरा नाम दिल्ली में हमारे कमरे के निकट के नगर-निगम के विद्यालय में लिखवा दिया गया और मुझे बारहखड़ी और संख्या ज्ञान की आधारभूत शिक्षा मिलने लगी। कक्षा-5 तक आते-आते मेरे बाल-मन में यह स्पष्ट हो चुका था कि इस विद्यालय की शिक्षा-प्रक्रिया और पद्धति दोनों ही ’अव्वल किस्म की लचर हालत में हैं और इसमें अधिक समय तक रहना अपने भविष्य को डुबाना है। विद्यालय में मेरा नाम भी छोटी उम्र में ही लिखवा दिया गया था और 3 वर्ष की उम्र में ही मैं कक्षा-1 का छात्र था। इसके लिए मेरी उम्र को एक साल अधिक दिखाने का गाँव का पुराना रिवाज भी बाकायदा अपनाया गया था। अब आप माने या ना माने, पर मुझे 8 वर्ष की उम्र में ही पता था कि मेरी शिक्षा महत्वपूर्ण है और इस विद्यालय में रहना बहुत घातक है।
शीतल अपने आलेख आजाद होने के लिए लड़ने में मदद और प्यार करना सिखाया में लिखती हैं-
कुछ यादें बस यादें ही नहीं होती, वह हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा होती है, जहाँ हम बार-बार जाना चाहते हैं। वे यादें और वहाँ बिताए पल जीना चाहते हैं । हमारा कल्पनाशील मन कई बार वहाँ घूमकर आ जाता है और कई बार उदास हो जाता है कि अब हम जहाँ जाना चाहते हैं या होना चाहते हैं, वहाँ नहीं हैं। कुछ ऐसी ही यादें मेरी लाइब्रेरी से जुड़ी हैं। कल्पनालोक में तो मैं हर वक्त खुद को उसके आसपास पाती हूँ। कक्षा नौ में जब मैं जी.आई.सी देवलथल गई। वहाँ पुस्तकालय ने धीरे-धीरे मुझे अपने पास बुलाया। पहले तो मैं चुपचुप और दबे पाँव लाइब्रेरी गई। पता ही नहीं चला कब बेखौफ और सिर ऊपर करके जाने लगी। वहाँ जाना अब अच्छा ही नहीं लगने लगा, बल्कि मेरा सबसे पसंदीदा वक्त में से एक बन गया। मुझे पता नहीं था लेकिन अब मैं वहाँ रखी किताबों के पन्ने पलटते लगी।
मुझे वहाँ की लाइब्रेरी में किताबों और पत्रिकाओं की भी कमी महसूस हुई। मुझे लगता है कि किसी भी स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी किताबें तलाशने की पूरी आजादी रहनी चाहिए। ताकि वह किताबें खोज सकें लेकिन वहाँ मैम बहुत टोकती हैं। जिससे चलते किताब पकड़ने में झिझक और डर लगता है। जब मैं और मेरी दोस्त जिला पुस्तकालय गए पहली बार तो हमें वहाँ बैठने को जगह ही नहीं मिली। इतने लोग आकर वहाँ पढ़ रहे थे कि एक भी ऐसा कोना नहीं था, जहाँ हम दोनों बैठ कर पढ़ सकते। हमने वहाँ से लौटने का फैसला किया। बाद में जानने वालों से पता चला कि वहाँ अगर बैठकर पढ़ना है तो सुबह जल्दी जाना होता है। वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे सुबह से ही आकर बैठ जाते हैं।
पुस्तकालय ने बताया कि यहाँ किताबों की दुनिया स्कूली किताबों की दुनिया से बहुत बड़ी है। इसके बाद पाठ्यपुस्तक पढ़ने में भी मजा आने लगा। पहले तक एक मजबूरी होती थी पढ़ना है और याद करना है । हमारा साथ दिया हमारी लाइब्रेरी ने, जिसने हमें नए शब्द दिए, नई जानकारियों और साथ-साथ नई कल्पनाओं से मिलाया।
आलोक कुमार मिश्र अपने अनुभवों को पुस्तकों से दोस्ती ने मुझे शिक्षक बना दिया में वह लिखते हैं-पुस्तकालयों ने न केवल पढ़ने के लिए ढेरों किताबें उपलब्ध कराई बल्कि पढ़ने औश्र पढ़े को बरतने का सलीका भी दिया। आज किताबें मेरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। नौकरी करते हुए मनपसंद किताबें खरीदकर पढ़ पाने की सलाहियत भी मिल गई है।
ऋचा जोशी घर के पुस्तक कोने से पुस्तकों के संसार में लिखती हैं- पिता को भिन्न-भिन्न किताबें पढ़ते हुए देखना और कुछ खास पुस्तकों की उपयोगी एवं रोमांचक विषयवस्तु पर यदा-कदा चर्चा करना दो महत्वपूर्ण कारक रहे जिन्होंने मुझे पुस्तकों के अनूठे संसार की ओर आकृष्ट किया। घर के पुस्तक कोने से गिजुभाई की पुस्तक ’दिवास्वप्न’ को मैंने अपनी पहली पुस्तक के रूप में चुना और गंभीरतापूर्वक पढ़ा। शिक्षा को बालकेंद्रित एवं रुचिकर बनाने के गिजुभाई के प्रयोगों ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया तथा मैंने सीखा कि पढ़ने का मकसद केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं होना चाहिए बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके पश्चात पाठ्यक्रम से अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह अनवरत जारी है और शायद थमेगा भी नहीं। प्रारंभिक दौर में मैंने अपने घर के पुस्तक कोने से अपनी रुचि के अनुसार अनुराधा बेनीवाल की ’आजादी मेरा ब्रांड’,सत्य व्यास की बनारस टाकीज, काशीनाथ द्वारा लिखित काशी का अस्सी, राबिन शर्मा की द मांक हू सोल्ड हिज फेरारी, तेत्सुको कुरोयोनागी की तोत्तोचान, चिंगिज एटमाटोव की पहला अध्यापक आदि पुस्तकें पढ़ीं।
दोस्त ने किताबों का चस्का लगाया में भूमिका पांडेय लिखती हैं-
बचपन से ही किताब पढ़ने में मेरी कोई खास रुचि नहीं थी। पढ़ाई ना करने के कारण या पढ़ते-पढ़ते सो जाने के कारण बचपन में अपने पिताजी के हाथों मैंने बहुत मार खायी है। अपने कॉलेज के दिनों में समाजशास्त्र से परास्नातक करने के दौरान भी अपने विषय से संबंधित पुस्तकें होने के बावजूद भी मैं परीक्षा के दिनों में अपने सहपाठी को कह दिया करती, यार तू मुझे इंपोर्टेट प्रश्न बता दे, मैं वही पढ़ लूंगी। हाँ, रुचि थी मुझे, तो सिर्फ क्लास में लेक्चर सुनने में या प्रेजेंटेशन देने में। कुछ नया जानने में, नए लोगों से मिलने में, नयी जगहों, नए लोगों, उनके जीवन और जीवन से जुड़े संघर्षो को जानने में। कई बार कोशिश करती उन्हें समझ कर समझाने की। ना जाने क्यों हमेशा से ही ये इच्छा रही कि मैं कुछ लिखूँ या कहीं बोलूँ तो लोग उसे पढ़ें, सुनें और सराहें।
एक समृद्ध पुस्तकालय का मालिक में सिद्दीक अहमद मेव लिखते हैं-
मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है, विशेषकर ऐतिहासिक कहानियाँ, उपन्यास आदि जब मैं प्राईमरी स्कूल में पढ़ता था हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी। कहानियों की किताबें, नेताओं की जीवनियाँ और उपन्यास। इस तरह पाँचवीं पास करते-करते मैंने कई सौ किताबें पढ़ डाली। इन किताबों में मुंशी प्रेमचंद, शेक्सपीयर, शरतचंद्र, गुलशननंदा, इब्नेशफी और सआदत हसन मंटो आदि बड़े लेखकों की किताबें भी थी।
इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, मुझे लगा मैं अपने सहपाठियों से काफी आगे हूँ। कई हमारे उस्ताद या कोई बाहर का आदमी कोई ऐसा सवाल पूछ लेता जो हमारे सलेबस से बाहर का होता तो मैं अक्सर उसका जवाब दे देता। यदि जवाब ठीक होता तो मुझे बहुत खुशी होती। इस तरह दिनों दिन मेरा पुस्तक प्रेम बढ़ता ही चला गया। परिणामस्वरूप मेरा सामान्य ज्ञान इतना बढ़ गया कि अपने सहपाठियों से ही नहीं बल्कि अपने सीनियरों से भी मैं सफल प्रतियोगिता करने लगा।
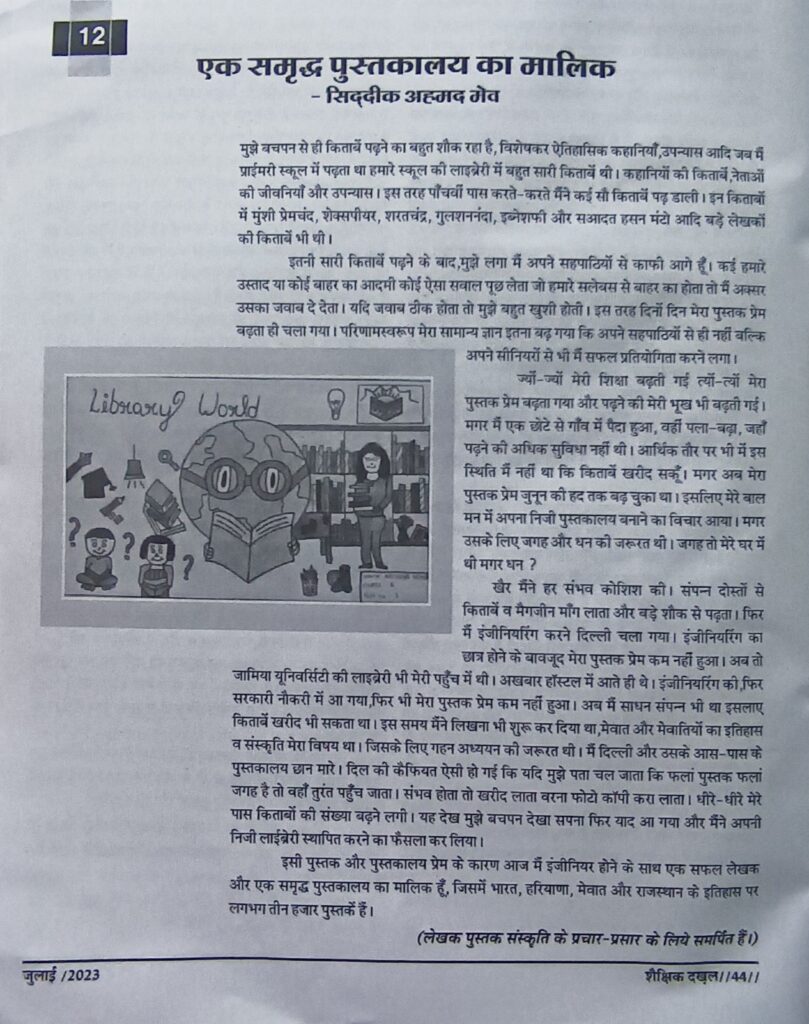
ज्यों-ज्यों मेरी शिक्षा बढ़ती गई त्यों-त्यों मेरा पुस्तक प्रेम बढ़ता गया और पढ़ने की मेरी भूख भी बढ़ती गई। मगर मैं एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ, वहीं पला-बढ़ा, जहाँ पढ़ने की अधिक सुविधा नहीं थी। आर्थिक तौर पर भी में इस स्थिति मैं नहीं था कि किताबें खरीद सकूँ। मगर अब मेरा पुस्तक प्रेम जुनून की हद तक बढ़ चुका था। इसलिए मेरे बाल मन में अपना निजी पुस्तकालय बनाने का विचार आया। मगर उसके लिए जगह और धन की जरूरत थी। जगह तो मेरे घर में थी मगर धन ?
किताबों की खुशबू की तरंगों के रास्ते लाइब्रेरी तक में कृति अटवाल लिखती हैं-
लिखना, पढ़ने की ओर ले जाता है। पढ़ने की भूख किताबों की खुशबू की तरंगों के रास्ते लाइब्रेरी तक पहुँचा देती है। यह तरंगें कुछ नया खोज लेने के आकर्षण से मुकम्मल हैं। लाइब्रेरी में मौजूद हर एक किताब में महफूज हैं किसी के विचार। किसी तबके की आवाज । किसी का मौन। किसी की कला। कहीं तसव्वुर के जहाँ में लगे गोते । और कहीं अंधेरे में लोप गुमनाम कहानियाँ। इन तक पहुँच थोड़ी कठिन है। पर अगर इनकी लत लग जाए तो पहुँच तक पहुँच बनाना भी आसान हो जाता है। मेरा भी लाइब्रेरी तक पहुँचने का सफर कुछ ऐसा ही रहा है। वह आगे लिखती हैं-कोविड की पहली लहर के दौरान गाँव में अत्यधिक फर्क नहीं पड़ा था। सभी बच्चे अपने घरों पर कैद जरूर थे। नतीजतन लाइब्रेरी का खुलना सभी के लिए वरदान साबित हुआ। यह पुस्तकालय मेरे लिए सबसे खूबसूरत था। कुदरत की गोद में लगने वाला यह अस्थायी पुस्तकालय था। गाँव में बच्चों ने पुस्तकालय कभी देखा ही नहीं था और जो चमक और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर पुस्तकालय में आकर आती थी वह अनमोल थी। इस पुस्तकालय ने मुझे किताबों की ताकत दिखाई। पुस्तकीय आकर्षण यूँ काम करने लगा कि जिसे पढ़ना पसंद नहीं है वह भी किताबों की ओर खींचा चला आया।
शायद ही मेरी व्याकरण सही होती में योगिता गोस्वामी लिखती हैं-
मेरे जीवन में पुस्तकालय की एक अहम भूमिका है। मुझे पुस्तकालय में जाना और वहाँ जाकर किताबों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पुस्तकालय में जाकर मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। जब मैं जूनियर कक्षा में थी, तब से ही मैंने पुस्तकालय जाना प्रारंभ किया। मैने जूनियर की शिक्षा नव ज्योति पब्लिक के विद्यालय से ली। उस विद्यालय में मैं प्रतिदिन पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ती थी, क्योंकि मैं व्याकरण में थोड़ी कच्ची थी। तो मैने वहाँ की सारी हिंदी व अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तकें पढ़ी और मुझे उनसे बहुत फायदा भी हुआ। 8वीं कक्षा के बाद मैनें विद्यालय बदला और विवेकानंद विद्या मंदिर में दाखिला लिया।

पूरन चंद अपने आलेख में कॉलेज में पुस्तकालय भी होता है लिखते हैं-
वर्ष 2017 की बात है। मैं एम. ए. अंग्रेजी की पढाई करने डी. एस. बी. परिसर नैनीताल गया, और मुझे वहा पर काफी अनुभवी एवं फीडम । वरिष्ठ शिक्षकों एवं मित्रों का साथ मिला। ये बारहवीं कक्षा के बाद मेरे लिए कॉलेज में एक छात्र के रूप में पहला अनुभव था क्योंकि बी. ए. की पढ़ाई मैंने एक व्यक्तिगत छात्र के रूप में की थी। डी.एस.बी. परिसर नैनीताल में दाखिला लेने के बाद मुझे पता चला कि कॉलेज में पुस्तकालय भी होता है, जिसमें छात्र-छात्राएँ बैठकर निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं। मैं चूँकि एक पिछड़े ग्रामीण इलाके से आया था कई सारी चीजें मेरे लिए बिलकुल नई थीं, यहाँ तक की अंग्रेजी विषय की पढ़ाई भी।
मुझे एक वाकया याद आ रहा है। हमारा एम.ए. का प्रथम लगभग पूरा हो चुका था और आतंरिक मूल्यांकन चल रहा था, सभी विद्यार्थियों को किसी एक प्रकरण पर प्रस्तुति देनी थी। जब मेरी बोलने की बारी आई तो में आगे गया और बोलने के लिए खड़ा हो गया, लगभग दो मिनट हो चुके थे मैं एक शब्द नहीं बोल पाया। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मेरी प्रोफेसर डॉ. हरिप्रिया पाठक का जिन्होंने बड़े ही नम्र भाव से और बड़े विश्वास के साथ कहा कि “मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ मुझे पता है तुम अच्छा बोल सकते हो।“ ये मेरे लिए घुटन के बाद एक लंबी साँस लेने जैसा अनुभव था और वही दिन था जब पहली बार मैंने पुस्तकालय का रुख किया। एक हफ्ते बाद मैंने फिर से अपनी प्रस्तुति दी हालाँकि बेहतर नहीं थी लेकिन मेरे प्रयासों को खूब सराहा गया।
लाइब्रेरी के साथ दिलचस्प सफर में रोहित भट्ट लिखते हैं-मैं कहना चाहूँगा कि किताबें पढ़ने में हर किसी को मजा आ सकता है, बस उसे उसकी पसंद मिलने की तलाश है। किताबें पढ़ने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। और हमारा आत्मविश्वास भी। और मुझे लगता है कि इसमें लाइब्रेरी बहुत बड़ा महत्व रखती है।
गायत्री बोरा मैं बनने की कहानी में अपने अनुभव से बताती हैं-मुझे बहुत मजा आता है ऐसी हास्य, व्यंग्यात्मक कहानियाँ पढ़ने में। ऐसी ही एक डायरी है जिसका नाम द डायरी आफ विम्पी किड इस डायरी के मैने 14 एडिशन डेढ़ महीने में खत्म कर दिए थे। मुझे लगता है कि अगर हमारे स्कूल में पुस्तकालय नहीं होता, तो शायद किताबों से मैं अच्छी तरह परिचित नहीं हो पाती। मैं कभी पुस्तकालय के बिना मैं नहीं बन पाती।
रिया चन्द्र खुद को पहचानना सिखाया में लिखती हैं- लाइब्रेरी में रौनक की लहर दौड़ पड़ती है। नन्हें कदमों के आते ही इंतजार में बैठी किताबें तैयार हो जाती हैं कोमल सी छुअन को महसूस करने के लिए। मिलन के इस खूबसूरत नजारे को देखती मेरी आँखें लाइब्रेरी के हर कोने में दौड़ने लगती हैं ताकि कोई कोना अनदेखा न रह जाए। दिनभर क्लास में व्यस्तता के बाद यह नजारा ठहरने का मौका देता है। एक कोने में बैठकर एकटक देखे रहने की माँग करता है। जिस लाइब्रेरी की कुछ समय पहले तक किसी को खबर न थी, वो आज बच्चों से ही गुलजार है।
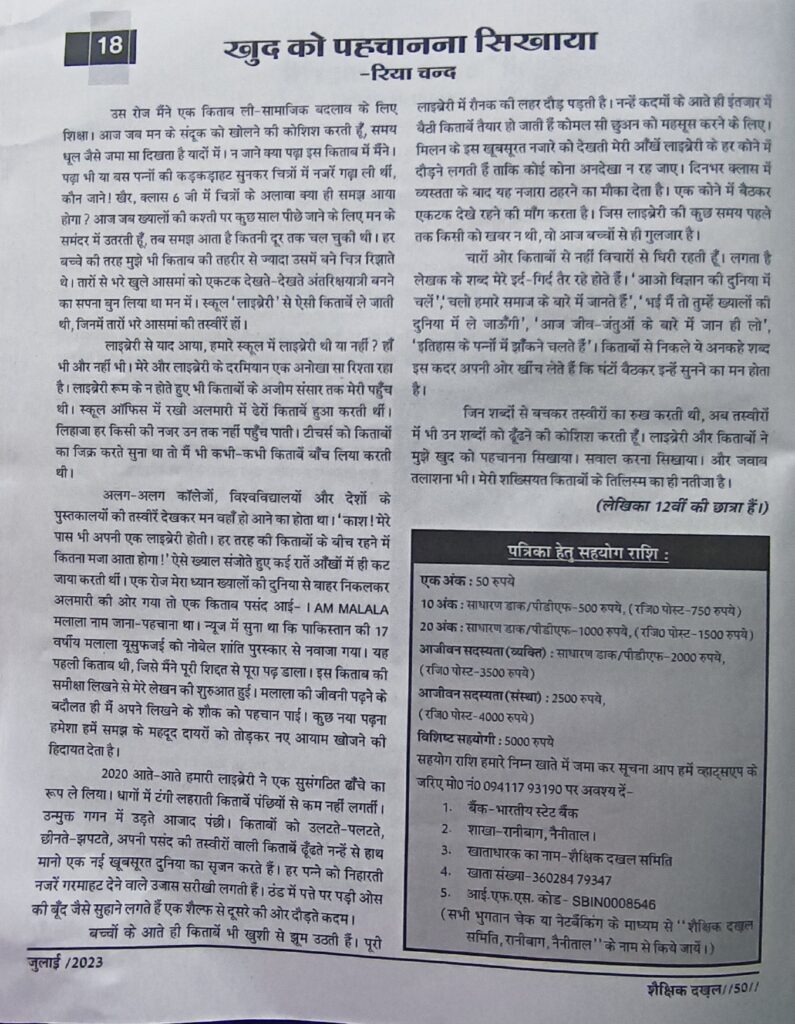
उस रोज मैंने एक किताब ली- सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा। आज जब मन के संदूक को खोलने की कोशिश करती हूँ, समय धूल जैसे जमा सा दिखता है यादों में न जाने क्या पढ़ा इस किताब में मैंने । पढ़ा भी या बस पन्नों की कड़कड़ाहट सुनकर चित्रों में नजरें गढ़ा ली थीं, कौन जाने ! खैर, क्लास 6 जी में चित्रों के अलावा क्या ही समझ आया होगा ? आज जब ख्यालों की कश्ती पर कुछ साल पीछे जाने के लिए मन के समंदर में उतरती हूँ, तब समझ आता है कितनी दूर तक चल चुकी थी। हर बच्चे की तरह मुझे भी किताब की तहरीर से ज्यादा उसमें बने चित्र रिझाते थे। तारों से भरे खुले आसमां को एकटक देखते-देखते अंतरिक्षयात्री बनने का सपना बुन लिया था मन में स्कूल ’लाइब्रेरी’ से ऐसी किताबें ले जाती थी, जिनमें तारों भरे आसमां की तस्वीरें हों।
हर किसी को जरूर इन नदी में डुबकी लगानी चाहिए में करनवीर सिंह लिखते हैं- अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि “शिक्षा तथ्य को सीखने के लिए नहीं बल्कि यह तो मन की सोच का प्रशिक्षण है।“ यह कथन आज की शिक्षा पर प्रश्नचिह्न लगाता है। वर्तमान की शिक्षा, रटने वाली प्रक्रिया के कुएँ में गोते खा रही है। इन सब के विपरीत हमारे स्कूल में बच्चों को लाइब्रेरी के नदी में गोते खाने का अवसर दिया जाता है। कुछ बच्चे तो अपने आप तैयार हो जाते हैं, इस नदी में जाने के लिए, मगर कुछ बच्चों को धक्का देना पड़ता है, क्योंकि वे इस नदी में नहाना पसंद नहीं करते हैं। पहले मैं भी इन्हीं में से एक विद्यार्थी हुआ करता था।
मुझे भी इस नदी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं इस नदी को देखते ही अपना मुँह मोड़ लिया करता था। मगर एक दिन मेरे कुछ साथी मुझे इस नदी के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि यह नदी बहारी स्वरूप से तो दूसरे नदियों जैसी नहीं है। परंतु जब हम इसमें डुबकी लगाते हैं तो हमें इस नदी की गहराई और अच्छाई का पता चलता है।
पंकज जोशी अपने आलेख लेखन और भाषाई दक्षता में बहुत बदलाव आया में लिखते हैं-अब तो मैंने कई किताबें पढ़ ली हैं और पढ़ने का सिलसिला जारी है। अब मेरी किताबों से दोस्ती होने लगी है। पहले मुझे लगता था कि मेरे साथ के सभी बच्चों को किताबें अच्छी कैसे लग सकती हैं? यह इतनी मोटी-मोटी किताबें इतनी आसानी से कैसे पढ़ लेते हैं?
किताबों ने मेरी समझ को काफी हद तक विकसित किया है। मेरे लेखन और भाषाई दक्षता में बहुत बदलाव आया है। साथ ही पढ़ने की आदत भी बनने लगी है। यह सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि मेरे आस-पास मुझे पढ़ने का वातावरण मिला। हमारी स्कूल लाइब्रेरी के कारण मेरी किताबों से दोस्ती हो पाई।
हर्ष कर्नाटक अपने अनुभव को किताबों से जुड़ने का सिलसिला में दर्ज करते हैं। वह लिखते हैं- मेरी पहली याद रह गई किताब ’किस्सा हातिमताई है। (यह एक काल्पनिक कथा है। एक राजा के पुत्र हातिमताई के ऊपर, हातिमताई ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में समर्पित कर दी थी।) यह मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है, क्योंकि इस किताब में हातिमताई एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैंने अभी तक इस किताब को दो बार फिर से पढ़ लिया है।
लॉकडाउन के समय खाली वक्त होने पर मैंने बहुत सी बाल कथाएँ, काल्पनिक कहानियाँ पढ़ी जिनमें से मुख्यतः जो मेरी पसंदीदा किताबें रही हैं। वह हैं- ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ भाग 1-2, हँस एंडरसन की कहानियाँ भाग 1-2, नार्निया भाग 1-3, अस्सी दिनों मैं दुनिया की सैर, हिंदी कहानियों के अलावा मैंने विज्ञान की भी किताबें पढ़ी।
मैंने यह किताबें अपने घर में स्थित लाइब्रेरी से पड़ी थी। पास में ही लाइब्रेरी होने का फायदा भी रहा कि कभी भी किताबें लाई जा सकती थी या लाइब्रेरी में ही पढ़ी जा सकती थी ।

मेरा पुस्तकालय से पहला परिचय भी घर में स्थित लाइब्रेरी से ही हुआ था। वर्षो पहले जब मेरे पिताजी ने लाइब्रेरी शुरू कर आसपास के बच्चों को हर रविवार एक निर्धारित समय पर किताबें पढ़ाई या घर पढ़ने के लिए दिए जाने का मौका दिया था तो मैंने भी इसमें भाग लेकर किताबें पढ़ना शुरू किया, जिसमें मेरा भी अच्छा मन लगा।
राजीव जोशी पढ़ने की संस्कृति, पुस्तकालय और कृष्ण कुमार का अध्ययन करते हैं और फिर उसे पढ़कर पुस्तकालय पर केन्द्रित कर एक शानदार लेख तैयार किया है। लगभग पन्द्रह अनुच्छेदों में सिमटा यह लेख काबिल-ए-गौर है। वह लिखते हैं-दक्षिण के राज्य बहुत आगे और अलग हैं। केरल राज्य में बच्चों को किताब उपलब्ध करवाने के लिए इन्स्ट्यिूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर आज भी है। वहाँ दशकों से गाँवों में किताबों का चलन है। बंगाल में पढ़ने की संस्कृति है।
परीक्षा का स्वरूप बदले, वह डराने के लिए न हो, किसी लोकतांत्रिक देश में परीक्षा बच्चों को शिक्षा के तंत्र के बाहर करने लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी शिक्षा में परीक्षा केंद्रित तंत्र लगातार मजबूत होता गया है। परीक्षा को पढ़ने की संस्कृति से अंतर्विरोध है।

जब स्टेट कमजोर होता है तो उसकी मार समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर पड़ती है। शिक्षा में निवेश घटने का असर पूरे स्कूल के साथ-साथ पुस्तकालय जैसी उप संस्थाओं पर भी पड़ता है। पूर्व सांसद आर॰के॰ नारायणन ने एक बार राज्य सभा में उदासी के स्वर में कहा कि हमने अपने बच्चों का बचपन छीन लिया है। एनसीएफ 2005 में जबरदस्त प्रतिरोध हुआ है। कई संस्थाएं निरन्तर इस ओर प्रयास कर रही हैं। आने वाला समय बताएगा कि हम कितना सफर तय कर पाए हैं।
शंकर लाल सैनी बाल पुस्तकालय में संवाद का स्थान में लिखते हैं- मानव जीवन में बाल्यकाल से ही शिक्षित होने, ज्ञानवर्धन एवं बौद्धिक विकास मे पुस्तकों का विशेष महत्व है मैंने भी प्राथमिक स्तर से महाविद्यालय तक के शिक्षण कार्य क्षेत्र में विद्यालय व महाविद्यालय के पुस्तकालय में वर्ण ज्ञान के साथ-साथ भौगोलिक, जैविक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा अध्ययन से जुड़ने की दिशा में मेरे अतिश्रेष्ठ गुरूजनों ने इस मुकाम तक पहुँचाने का कार्य किया। सन् 2005 में राजकीय सेवा मे अध्यापक पद पर चयन होने के पश्चात सर्वप्रथम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, साडागाँव (टोंक राजस्थान) में नौनिहाल विद्यार्थियों के साथ शिक्षण कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, विद्यार्थियों के पठन-पाठन प्रक्रिया के साथ-साथ स्थानीय विद्यालय के पुस्तकालय के माध्यम से संक्षिप्त पठन सामग्री, रोचक व लगन पैदा करने वाली कहानियाँ, कविताएँ, रंगीन सचित्र पुस्तकों के माध्यम से सरल भाषा में ज्ञानशील एवं विद्यार्थियों के परिवेश से जुड़ी होने के कारण रूचिकर हुई।
हिमांशु जोशी एक जानकारीपरक यात्रावृत्तांत लाए हैं। उत्तराखण्ड का पहला पुस्तकालय गाँव में लिखते हैं- उत्तराखंड स्थित ’गाँव घर फाउंडेशन’ ने पर्यटन और किताबों का अद्भुत मेल करने की ठानी और मणिगुह को पुस्तकालय गाँव बना दिया। उनके द्वारा किताबों को मंदिर से जोड़ दिया गया है ताकि लोग किताबों को धर्म से जोड़ने लगें। उत्तराखंड की सुंदर और शांत पहाड़ियों को यदि इस तरह कला, पुस्तकालय से जोड़ दिया जाए तो प्रदेश का पर्यटन दोगुनी रफ्तार पकड़ लेगा। इसका उदाहरण लेते हुए प्रति और किताबों का यह मेल हमारे देश की तस्वीर भी बदल सकता है। ’गाँव घर फाउंडेशन’ चार लोगों का फाउंडेशन है। जिसमें ’रेख़्ता फाउंडेशन की पहल सूफीनामा से जुड़े सुमन मिश्रा, उनकी पत्नी बीना नेगी, आलोक सोनी और राहुल रावत शामिल हैं। बीना नेगी और राहुल रावत उत्तराखंड से पलायन कर दिल्ली में बसने वाले उन करोड़ों उत्तराखंडियों में से हैं, जिनके पिता मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गाँव से पलायन कर दिल्ली में बस गए। आलोक सोनी मीडिया जगत में जाना-माना नाम हैं, वह हिंदुस्तान टाइम्स से लंबे समय तक जुड़े रहे।
मुकेश नौटियाल कृत अनुभव दक्षिण भारत में पुस्तक संस्कृति भी पठनीय है। वह लिखते हैं- अपनी पुस्तक ’कालड़ी से केदार’ को लिखने से पहले मैंने दक्षिण भारत की दो सघन यात्राएँ की। पहली यात्रा साल 2013 में और दूसरी यात्रा साल 2018 में संपन्न हुई। ये दोनों यात्राएँ दक्षिण भारत की संस्कृति, साहित्य, कला और परंपरा को परखने के प्रयोजन से की गई थीं। इस यात्रा में मैंने आम से लेकर खास लोगों से मुलाकातें कीं और वहाँ के रचनात्मक पहलुओं को टटोलने की कोशिश की।
बेंगलुरु पहुँचने पर पता चला कि यह दरअसल एक छोटा भारत है, जहाँ देशभर के अनेक प्रांतों से लोग, खासकर प्रोफेशनल युवा रोजगार के लिए आते हैं । यहाँ बेशक कन्नड़ संस्कृति प्रधान है लेकिन थोड़ा-थोड़ा सभी राज्यों का अंश यहाँ देखा जा सकता है।
एक रेस्टोरेंट में मैंने देखा कि आलीशान और विशाल डाइनिंग टेबल के करीब पुस्तकों की अलमारी रखी हुई है। उस अलमारी में लगभग सभी किताबें अंग्रेजी भाषा की थीं। यह जानकर सुकून मिला कि कई लोग उस खुली अलमारी को टटोलने और अपनी पसंद की किताब लेने के लिए आगे आ रहे थे। जाहिर है, ऑर्डर डिलीवर होने से पहले अल्प समयांतराल में पाठक किताब पूरी नहीं पढ़ सकते लेकिन उसकी तासीर तो महसूस कर ही सकते हैं।
दिनेश जोशी संगोष्ठी की रपट लाए हैं। कुछ अंश- राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड शाखा जनपद नैनीताल के अकादमिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता श्री मदन मोहन पांडे (लेखक और शिक्षक पूर्व प्रवक्ता एससीईआरटी देहरादून) ने कहा कि पूरी सरकारी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की हर चीज़ में केंद्रीकरण की पद्धति हावी हो गई है। सब कुछ ऊपर से संचालित करने की प्रवृत्ति ही सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा विभागों का हाल है कि उसके शीर्ष अधिकारी और नीति-निर्माता अपने ही शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित करने के मौके तलाशते रहते हैं। यह ऐसी सेना बन गई है, जिसका कमांडर हर समय अपने सैनिक की हिम्मत बढ़ाने की जगह उन्हें ही हर बात के लिए दोषी सिद्ध करने का जतन करता रहता है। फिर कहता है कि परिणाम अनुकूल नहीं आ रहे हैं। शिक्षक का अधिकांश समय अभिलेखीकरण में खर्च करवा दिया जाता है। जिसके लिए लिपिक का पद होता है पर अधिकांश अभिलेखीकरण का कार्य शिक्षकों के ऊपर थोप दिया गया है। शिक्षक के पास न तो अपने विषय को पढ़ाने का पर्याप्त समय उपलब्ध है न ही बच्चों को जानने, समझने और आंकलन तथा मूल्यांकन का समय है। कई शोध कहते हैं कि बार-बार मासिक परीक्षा की कोई जरूरत नहीं। बोझिल और अनियोजित परीक्षा बेहद नकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। परीक्षाओं का बोझ कम करने की बात तो बहुत होती है पर इसके उलट परीक्षाओं की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है।
अफलातून विष्णु की अफलातून की डायरी भी खास है। एक बानगी-
08.01.2022 ’सरकारी स्कूल में निजी लाइब्रेरी’ शीर्षक से भाई अभिनव सरोवा का एक साक्षात्कार सुना। फेसबुक के जरिए परिचय उनसे पहले से था। अभी संगमन में मुलाकात भी हो गई। तो उस साक्षात्कार में वे प्रश्नकर्ता के पूछे जाने पर कि आपके मन में ये खयाल नहीं आया कि “कहीं किताबें कोई चुरा ले गया तो ?“ अभिनव अपने खांटी देशी अंदाज में उत्तर देते हैं कि “किताबें चुराने वाले लोग इस देश में रहे कहाँ हैं साहब ?”… अभिनव से आईडिया लेकर मैंने भी अपने कॉलेज में निजी लाइब्रेरी खोलने का मन बनाया लेकिन कोई कमरा उपलब्ध नहीं था। विचार मन को मथता रहा। तभी एक दिन कैम्पस में घूमते हुए विचार आया कि सीढ़ियों के नीचे के एक कोने में ही क्यों न ओपन लाइब्रेरी खोली जाए ? आईडिया पिं्रसिपल सर को बताया तो उन्होंने झट सहमति दे दी। फिर अन्य साथियों को आईडिया सुनाया तो भिड़ते ही वही सवाल-‘“बच्चे किताबें चुरा ले जाएँगे… आप जानते नहीं यहाँ के बच्चों को ।
मैंने भी अभिनव का उत्तर दोहरा दिया- “किताबें चुराने वाले लोग इस देश में रहे कहाँ हैं साहब ? “….
दूसरा सवाल – “ किताबें कहाँ से आएँगी ?“
’मैं खुद लेकर आऊँगा.’ “
’और बच्चे ले गए तो ? “
’और ले आऊँगा. “
“फिर ठीक है.
शिरीष खरे पुस्तकालय के क्षेत्र में हिन्दी प्रयोगशाला में अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त करते हैं- किताबों वाली जगह को पुस्तकालय कहा जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ किताबों वाली जगह को ’हिन्दी प्रयोगशाला’ कहते हैं। यह जगह है राजस्थान के झुंझनूं जिले के एक छोटे से गाँव पीथूसर के सरकारी स्कूल में, और इस जगह को तैयार किया है यहाँ के हिन्दी शिक्षक अभिनव सरोवा ने अभिनव बताते हैं कि स्कूलों में हिन्दी भाषा संबंधी विषय के लिए पुस्तकालय होता है, जबकि विज्ञान जैसे विषय के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है, लेकिन उन्होंने हिन्दी भाषा में एक नए विजन को लेकर प्रयोग किया है, लिहाजा नाम दिया है- ’हिन्दी प्रयोगशाला।’
’हिन्दी प्रयोगशाला’ के अंदर बीते दस-बारह वर्षों में हजार से बारह सौ हिन्दी की किताबें शामिल हो चुकी हैं। इसमें से कई किताबें अभिनव ने खुद खरीदी हैं तो कई सारी किताबें उन्हें उपहार के तौर पर भी मिली हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों का समय बचाने और उन्हें किताबों की दुनिया में ले जाने के लिए किए गए इस प्रयोग के बारे में अभिनव कहते हैं कि किताबें ज्ञान का भंडार तो होती ही हैं, लेकिन यदि हम लगातार किताबों से जुड़े रहे तो सोचकर बोलते हैं और किसी भी प्रश्न पर भड़कते नहीं हैं। कारण है कि लगातार किताबों को पढ़ने से हमारे अंदर मानसिक तौर पर एक स्थिरता आ जाती है और यही मानसिक स्थिरता से एक दृष्टि बनती है, जिसका लाभ हमें आम जीवन में मिलता है। ’हिन्दी प्रयोगशाला’ के चलते बच्चे पाठ्यक्रम से बाहर की किताबों को भी पढ़ रहे हैं और वे सावित्री बाई फुले आदि व्यक्तित्वों के बारे में जानने के लिए किताबों को माँग कर घर ले जा रहे हैं।
हेम पंत ने हिमांशु कफलटिया से शानदार बातचीत की है। दो अंश-
‘‘मैंने अपने अनुभवों से जाना है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों की बहुत कमी है। खुद हमको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ा। सेवा में आने के शुरुआती सालों में मैंने उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में प्रशिक्षण लिया और सितंबर 2020 में पूर्णागिरी तहसील में उपजिलाधिकारी के पद पर नियुक्ति मिलते ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों की सुविधा के लिए तहसील परिसर में ही ’सिटीजन लाइब्रेरी’ की शुरुआत की। युवाओं की बढ़ती संख्या को देखकर जल्दी ही हमने नगरपालिका टनकपुर में अगली शाखा खोली। दूर गाँवों से आने वाले युवाओं की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए टनकपुर और बनबसा के आसपास के कई गाँवों में ऐसे पुस्तकालय खोले गए। अब हमने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए चंपावत जिले के बाद नैनीताल जिले के दूरस्थ इलाके में खनस्यू और नाई गाँवों में भी पुस्तकालय शुरू कर दिए हैं। गढ़वाल के कुछ जिलों में भी शुरुआत हो चुकी है।’’
‘‘शुरुआत में जो पुस्तकालय खोले गए उनमें आने वाले अधिकांश छात्र वो थे, जिनको पढ़ने के लिए शांत माहौल, किताबों और सामूहिक तैयारी की जरूरत होती थी। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि तहसील परिसर में दिन रात किसी भी समय आकर बच्चे पढ़ सकें। अब जो पुस्तकालय गाँवों में खोले जा रहे हैं, वहाँ छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जरूरत के अनुसार लोकप्रिय साहित्य और अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही हैं।’’
विप्लवी पुस्तकालय-जन चेतना की मशाल को कौशल किशोर की फेसबुक भित्ति से साभार लिया गया है। एक अंश-
यह महज पुस्तकालय नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर वर्तमान के सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक आंदोलन की धरोहर को अपने में समेटे है। इसकी नींव स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 26 फरवरी 1931 को पड़ी थी। यह उस संघर्ष और कुर्बानी के इतिहास का गवाह है। आजादी के बाद की पीढ़ी ने इसे खंडहर होने से बचाया है तथा संवारा और आधुनिक रंग-रूप दिया है।
गोदरगावां कथाकार, उपन्यासकार व साम्यवादी नेता राजेंद्र सजन का गाँव है। विप्लवी पुस्तकालय उनकी कल्पनाशीलता, जन प्रतिवद्धता और सांस्कृतिक सरोकार का मूर्त रूप है। पुस्तकालय को उन्होंने संस्थाबद्ध किया है। एक टीम के पास संचालन की जिम्मेदारी है। यहाँ लोकतांत्रिक माहौल है। ऐसे समय में जब पुस्तकालय संस्कृति संकट में है, वे नष्ट किए जा रहे हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है, विप्लवी पुस्तकालय एक मशाल की तरह है। यह हम जैसों के लिए किसी साहित्यिक तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। वहाँ 2 दिन के प्रवास के दौरान यही महसूस होता रहा है।
देवेन्द्र मेवाड़ी की प्रस्तुति पढ़ाकू अन्ना मणी भी अंक में है। एक अंश- अन्ना मोदाइल मणी हमारे देश की प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थीं। उनका जन्म 23 अगस्त 1918 को त्रावणकोर, केरल में हुआ था। उन्हें पढ़ने की बहुत लगन थी। कहा जाता है, जब वे 8 वर्ष की थीं तो उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी की मलयालम भाषा की सभी पुस्तकें पढ़ ली थीं। और, जब वे 12 वर्ष की हो गई तो उन्होंने उस लाइब्रेरी की अंग्रेजी भाषा की सभी पुस्तकें पढ़ ली। उन्हें पुस्तकें पढ़ने की इतनी लगन थी कि माता-पिता ने जब उनके आठवें जन्मदिन पर अन्य बेटियों की तरह उन्हें भी हीरे के कर्णफूल देने चाहे तो अन्ना मणी ने मना कर दिया। माता-पिता ने पूछा- तो बेटी तुम्हें क्या चाहिए? अन्ना मणी ने कहा- मुझे एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का सेट चाहिए।
प्रख्यात कथाकार दिनेश कर्नाटक की कहानी भी अंक में है। सार्वजनिक सम्पत्तियों को समाज कितना और किस तरह का बेकार समझता है! अराजक लोग किस तरह स्कूल जैसी संस्था के परिसर को बरबाद करने पर तुले हैं! कैसे और क्यों शिक्षक फिर उदासीन हो जाते हैं ! फिर समाधान क्या हो? कैसे व्यवस्थाएँ सुधरेंगी? यह कहानी विचलित करती है। यह पाठक को उसकी भूमिका और उसके कार्य व्यवहार को भी चुनौती देती है। आप भी पढ़िएगा ‘एक नए मुल्ला का पुस्तक प्रेम।’ कुछ अंश-
आखिरकार राजीव ने अध्यापकी को चुना। स्कूल उन्हें बचपन में बिलकुल पसंद नहीं था। मगर अब उन्हें स्कूल से जुड़ने तथा शिक्षक होने में जीवन का अर्थ नजर आ रहा था। इन वर्षों में सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हुए उन्हें तथाकथित कामयाबी की निरर्थकता समझ में आ गई थी। स्कूल के माहौल में एक खास तरह की सरलता व सहजता थी। बच्चों का साथ था, जिनकी निश्छलता, अनगढ़ता उन्हें प्रिय थी। और वे सभी अच्छी बातें और विचार जिन से इंसान और दुनिया अच्छी होती थी, उन्हें बच्चों तक पहुँचाने का मौका था। सब से बढ़कर स्कूल में किताबें थी । किताबें उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। किताबों से उन्हें उसी तरह का लगाव था जैसा किसी गायक को संगीत से, किसी चित्रकार को रंग और कैनवस से और किसी खिलाड़ी को खेल के मैदान से होता है। किताबें ही उन्हें वापस उस स्कूल की ओर लेकर आई थी, जो कभी उन्हें सख्त नापसंद था और कैदखाने जैसा लगता था । किताबों ने ही उन्हें समझाया था कि स्कूल को कैदखाने की तरह नहीं किसी बाग की तरह खुशनुमा होना चाहिए। किताबें उन्हें निरंतर जीवन को जानने-समझने के सूत्र देती रहती थी। ये किताबें ही थी जिन्हें पढ़कर तथा बगैर कोई यात्रा किए उन्होंने देश-दुनिया के लोगों, गाँवों, कस्बों, शहरों, रीति-रिवाजों, सुख-दुख, संघर्ष व चिन्ता को जाना था। विशेष रूप से खूब बांग्ला व रूसी साहित्य पढ़ने के कारण उन्हें बंगाल व रूस का जन-जीवन परिचित सा लगता था।
उनका मकसद साफ था, जिन किताबों को उन्होंने दुनिया की बेहतरीन चीज के रूप में जाना था, उनके जरिए बच्चे सही मायने में शिक्षित हों। बच्चे प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्द्धाओं में पड़कर नाराज, उदास और कुंठित होने के बजाय सहयोग, सदभाव तथा खुशी के रास्ते पर चलें। हालांकि वे जानते थे समय का प्रवाह उनके पक्ष में नहीं है। लोग अच्छाई की बातें करना जरूर पसंद करते थे, उसके समाप्त होते जाने पर रूदन करते थे, मगर जिन चीजों की बुराई करते, खुद वही सब करते। माँ-बाप भी बच्चों को स्कूल जीवन को जानने-समझने और बेहतर इंसान बनने के बजाय इस उद्देश्य के साथ भेजते की आगे जाकर वह अपने लिए नौकरी का बंदोबस्त कर सकें।
उन्होंने गौर किया कि धीरे-धीरे पहले की तरह उनके भतर टट्टी को देखकर घृणा उत्पन्न नहीं होती, न जी मिचलाता है, न गुस्सा आता है, न शिकायत करने का मन होता है। धीरे-धीरे समझ बन रही थी कि जिस काम को आप अच्छा और जरूरी समझते हों, जरूरी नहीं कि दूसरे लोग भी समझें। तो परेशानी किस बात की। आप अपना काम करो, वह अपना काम करें।
अन्तिम बाहरी आवरण में शुभनीत कौशिक का अनुभव किताबों का सम्मोहन भी है।

कुछ अंश आपके लिए यहाँ दिए जा रहे हैं- किताबों का अपना दुर्निवार आकर्षण होता है। ये वही समझ सकता है, जिसे किताबों के सम्मोहन ने बिंध रखा है। आपको पता भी नहीं चलता कि किताबों के प्रति कब वह सम्मोहन कब धीरे-धीरे ऑब्सेशन में बदल जाता है। घर में, आपके निजी संग्रह में देनों ऐसी किताबें है, जिन्हें अभी पढ़ना बाकी है, इस बात का अंदाजा आपको भी बखूबी है, लेकिन आप नई किताबें खरीदने से खुद को रोक नहीं पाते।
किताबों का वह सम्मोहन खुद मेरे लिए ऑब्सेशन की हद तक चला जाता है। बिना पढ़ी हुई किताबों की बढ़ती हुई फेहरिस्त को देखता हूँ तो हम जार तय करता हूँ कि अब कम-से-कम दो तीन महीने किताबें नहीं खरीदूंगा। लेकिन किताबों के सामने आते ही सारा तय किया हुआ धरा रह जाता है नतीजा कुछ और किताबें संग्रह में जुड़ जाती हैं। मोबाइल के नोट्स में मैने एक फाइल बना रखी है’ बुक्स टु बाई’ नाम से। जिसमें उन किताबों के नाम में जोड़ता रहता हूँ, जिनकी समीक्षाएँ मुझे अच्छी लगती है, जिनके विषय मुझे पसंद आते है या फिर जिनका जान मेरा कोई दोस्त सुजाता है यानी फेरिस्त उन किताबों की, जिन्हें भविष्य में पड़ने का मेरा मन है।
किताबों का यह सम्मोहन कई बार आपको ऐसी जगहों तक ले जाता है, जहाँ आप अन्यथा नहीं जाते दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद की यात्रा से तो किताबों के ठिकानों तक पहुँचने के लिए समय निकालना। किताबों के इसी सम्मोहन ने मेरा परिचय दरियागंज और वहाँ लगने वाली ’संडे बुक मार्केट’ में कराया। जेएनयू में रहते हुए कई बार ऐसा भी हुआ कि रविवार को नैं दरियागंज पहुँचा और पता चला कि आज मार्केट नहीं लगी है फिर निराश होकर वापस लौटना। इस बार संपादकद्वय का एक हिस्सा पत्रिका में नहीं है।
पत्रिका: शैक्षिक दख़ल, छमाही
संपादक: महेश पुनेठा-दिनेश कर्नाटक
वर्ष: 12
अंक: 22
मूल्य: 50 रुपए
प्रकाशक: शैक्षिक दख़ल समिति
सम्पर्क: 941707470,9411793190,9411347601
समेकन: मनोहर चमोली ‘मनु’
सम्पर्क: 7579111144